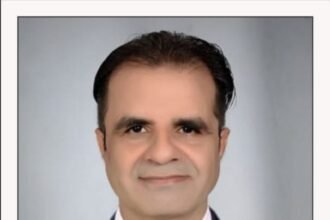लेखक: कर्नल देव आनंद लोहामरोड़
सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ
इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में विश्व जिस तेज़ी से एक बार फिर महाशक्ति प्रतिस्पर्धा की ओर लौटता दिख रहा है, उसमें ग्रीनलैंड जैसे दूरस्थ, बर्फ़ से ढके और कम आबादी वाले द्वीप का अचानक वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ जाना कोई संयोग नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार-बार यह कहना कि अमेरिका को ग्रीनलैंड “चाहिए” या “किसी न किसी तरह उसे हासिल करना होगा”, पहली नज़र में भले ही एक सनकी और अव्यावहारिक बयान लगे, लेकिन इसके पीछे लगभग दो सदियों से चली आ रही अमेरिकी रणनीतिक सोच, आर्कटिक क्षेत्र का बदलता भू-राजनीतिक महत्व और चीन-रूस के उभार से पैदा हुई असुरक्षा की गहरी छाया साफ़ दिखाई देती है। असल प्रश्न यह नहीं है कि ग्रीनलैंड बिकेगा या नहीं, क्योंकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर चुके हैं। असल प्रश्न यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर प्रभाव-क्षेत्रों की राजनीति की ओर लौट रही है और क्या आर्कटिक क्षेत्र आने वाले समय का नया रणनीतिक रणक्षेत्र बनने जा रहा है।
ग्रीनलैंड भले ही देखने में बर्फ़ और हिमनदों से ढका एक वीरान द्वीप प्रतीत हो, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति उसे असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बना देती है। यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है और आर्कटिक महासागर तक पहुँच का एक प्राकृतिक द्वार है। शीत युद्ध के दौर से ही यह क्षेत्र अमेरिकी मिसाइल चेतावनी प्रणाली और सामरिक निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आज जब जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, तब इस पूरे क्षेत्र का आर्थिक और सामरिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। जिन मार्गों से पहले केवल परमाणु पनडुब्बियाँ और सैन्य जहाज़ गुज़रते थे, अब वहाँ से वाणिज्यिक जहाज़ों के गुजरने की संभावनाएँ बन रही हैं। इसके साथ ही, आर्कटिक क्षेत्र में दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तेल और गैस के विशाल भंडार होने की संभावनाएँ भी वैश्विक शक्तियों को आकर्षित कर रही हैं।
अमेरिका की ग्रीनलैंड में रुचि कोई नई बात नहीं है। यह रुचि लगभग दो सौ साल पुरानी है। उन्नीसवीं सदी में, जब अमेरिका “क्षेत्रीय विस्तार” की नीति के तहत एक महाद्वीपीय शक्ति से वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा था, तब से ही ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर उसकी नज़र थी। 1867 में जब अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा, उसी दौर में अमेरिकी नीति-निर्माताओं ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड को भी अमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र में लाने की संभावनाओं पर विचार किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ग्रीनलैंड की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच समुद्री और हवाई मार्गों की सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक चौकी था।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब नाज़ी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्ज़ा कर लिया था, तब अमेरिका ने यह सुनिश्चित किया कि ग्रीनलैंड जर्मन नियंत्रण में न जाए। इसी दौरान वहाँ अमेरिकी सैन्य उपस्थिति स्थापित हुई। युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध शुरू हुआ और सोवियत संघ अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन गया, तब ग्रीनलैंड नाटो की “उत्तरी ढाल” का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 1951 में डेनमार्क और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद वहाँ जिस एयर बेस की स्थापना हुई, वही आज पिटुफिक स्पेस बेस के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के दौर में यह बेस सोवियत मिसाइल गतिविधियों की निगरानी और अमेरिकी परमाणु चेतावनी प्रणाली का एक अहम केंद्र था। यानी, कानूनी रूप से चाहे ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन रहा हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से वह दशकों से अमेरिकी रणनीतिक तंत्र का हिस्सा रहा है।
1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का औपचारिक प्रस्ताव दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका इस द्वीप को कितनी गंभीरता से लेता रहा है। डेनमार्क ने उस समय इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन अमेरिकी रणनीतिक सोच में ग्रीनलैंड का महत्व कभी कम नहीं हुआ। शीत युद्ध के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि इस क्षेत्र का सामरिक महत्व घट गया है, लेकिन इक्कीसवीं सदी में परिस्थितियाँ फिर से बदलने लगीं।
आज तीन बड़े कारक आर्कटिक क्षेत्र को फिर से वैश्विक राजनीति के केंद्र में ले आए हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन, जिसने बर्फ़ को पिघलाकर नए समुद्री मार्ग खोल दिए हैं और संसाधनों तक पहुँच आसान बना दी है। दूसरा, चीन का उदय, जो अब स्वयं को “नियर-आर्कटिक स्टेट” कहता है और आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक, आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, रूस, जो अपने उत्तरी तट और आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य ढांचे को मज़बूत कर रहा है और इसे अपनी सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा मानता है।
इन्हीं परिस्थितियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान सामने आते हैं। 2019 में जब उन्होंने पहली बार इसे “खरीदने” की इच्छा जताई थी, तब पूरी दुनिया ने इसे एक अजीब और अव्यावहारिक विचार माना। लेकिन ट्रंप की राजनीति की विशेषता यही है कि वह जटिल भू-राजनीतिक मुद्दों को भी रियल एस्टेट सौदे की भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके दृष्टिकोण से देखें तो ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथ में होगा तो न चीन वहाँ पैर जमा सकेगा और न ही रूस को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने इस मुद्दे पर और भी आक्रामक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे यूरोप में यह चिंता गहराने लगी है कि क्या अमेरिका अब अपने ही सहयोगियों की संप्रभुता पर दबाव बनाने से भी नहीं हिचकेगा।
यही टकराव जनवरी 2026 में एक नए और कहीं अधिक खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया। 17 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने रुख का विरोध करने वाले देशों के खिलाफ खुला आर्थिक दबाव बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो देश अमेरिका की इस रणनीति में “बाधा” डालेंगे, उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसके तहत अमेरिका ने डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और नीदरलैंड्स सहित कई यूरोपीय देशों के सामानों पर 1 फरवरी 2026 से 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, जिसे यदि राजनीतिक सहमति नहीं बनती है तो 1 जून 2026 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक किया जा सकता है। यह कदम स्पष्ट रूप से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी रणनीतिक हितों के खिलाफ यूरोप के विरोध का जवाब है। यूरोपीय देशों ने दो टूक कहा है कि ग्रीनलैंड कोई बिकाऊ संपत्ति नहीं है और उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह विवाद अब केवल राजनीतिक या सामरिक न रहकर एक बड़े ट्रांस-अटलांटिक व्यापार और कूटनीतिक टकराव का रूप लेने लगा है, जिसका असर आने वाले समय में अमेरिका-यूरोप संबंधों और वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर गहराई से पड़ सकता है।
यहाँ एक ज़रूरी तथ्यात्मक संतुलन समझना आवश्यक है। यह सही है कि रूस आर्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और चीन वहाँ आर्थिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियाँ तेज़ कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि चीन या रूस ग्रीनलैंड पर सीधे कब्ज़ा करने की योजना बना रहे हों। उनकी रुचि मुख्यतः समुद्री मार्गों, संसाधनों और दीर्घकालिक रणनीतिक पहुँच तक सीमित है। फिर भी, अमेरिका इसे भविष्य के खतरे के रूप में देख रहा है और शायद इसी कारण वह इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मज़बूत करना चाहता है।
डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों का रुख इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट और सख्त है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और उसका भविष्य वहाँ के लोगों की इच्छा से तय होगा। ग्रीनलैंड में स्वतंत्रता की भावना ज़रूर मौजूद है, लेकिन वह स्वतंत्रता डेनमार्क से राजनीतिक रूप से अलग होने की कल्पना से जुड़ी है, न कि किसी दूसरी महाशक्ति के अधीन जाने से। वहाँ की जनता और नेतृत्व दोनों इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उनकी सुरक्षा और भविष्य नाटो जैसे बहुपक्षीय ढांचे के भीतर ही सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
यहीं पर नाटो का प्रश्न सामने आता है। ग्रीनलैंड पहले से ही नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य है। यदि रूस या चीन से कोई वास्तविक और प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न होता है, तो उसका जवाब सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के तहत दिया जा सकता है। ऐसे में किसी क्षेत्र को “खरीदने” या उस पर राजनीतिक दबाव डालने की नीति न केवल अनावश्यक है, बल्कि वह उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को भी कमजोर करती है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वयं अमेरिका ने गढ़ा था।
यह पूरा विवाद हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जिस वैश्विक व्यवस्था की नींव रखी थी, उसकी बुनियाद थी—संप्रभुता का सम्मान, सीमाओं की पवित्रता और लोकतांत्रिक आत्म-निर्णय का सिद्धांत। यदि आज वही अमेरिका अपने एक लोकतांत्रिक सहयोगी पर दबाव डालकर उसकी ज़मीन “हासिल करने” की भाषा बोलता है, तो यह केवल डेनमार्क या ग्रीनलैंड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है।
वास्तव में, ग्रीनलैंड का मुद्दा केवल एक द्वीप का मुद्दा नहीं है। यह उस दुनिया का संकेत है, जहाँ नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था धीरे-धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है और उसकी जगह शक्ति-आधारित राजनीति वापस लौट रही है। यह उस भविष्य की झलक है, जहाँ जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की होड़ और रणनीतिक मार्गों पर नियंत्रण की इच्छा नई तरह की प्रतिस्पर्धा और टकराव को जन्म दे सकती है।
अंततः प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका कितना शक्तिशाली है या चीन और रूस कितनी तेज़ी से उभर रहे हैं। असली प्रश्न यह है कि क्या दुनिया उन सिद्धांतों पर टिकी रहेगी, जिन पर पिछले आठ दशकों से सापेक्षिक स्थिरता बनी हुई थी, या फिर हम एक बार फिर उस युग की ओर लौटेंगे, जहाँ ताकत ही न्याय का एकमात्र मापदंड हुआ करती थी। ग्रीनलैंड आज इसी बड़े परिवर्तन का प्रतीक बन गया है।